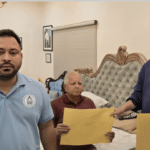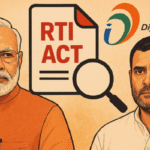सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर 2025) को अपने ही 2014 के उस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) से छूट दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि कई संस्थान केवल इस कानून से बचने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की। यह छूट समान शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक समावेशिता के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकती है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट (Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
उन्होंने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए कहा कि 2014 का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 30(1) (अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापित करने का अधिकार) के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर रहा है। हालाँकि कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों अनुच्छेद एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं और इन्हें समन्वय के साथ लागू किया जा सकता है।
पीठ ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि RTE की जिम्मेदारियों से बचने के लिए संस्थानों का खुद को अल्पसंख्यक घोषित करना कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर रहा है।
साथ ही RTE के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) जैसी गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली शर्तें भी इन संस्थानों पर लागू नहीं होतीं। इसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) क्या है?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (Right to Education Act) भारत सरकार की ओर से पारित एक कानून है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
इस कानून की धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा में सभी वर्गों के लिए समानता और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना है।

2014 के फैसले पर उठे सवाल
पीठ ने 2014 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (Pramati Educational and Cultural Trust) बनाम भारत संघ के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की नींव को कमजोर कर सकता है। साथ ही इससे समाज में अलग-अलग वर्गों में बँटवारा हो सकता है और असमानता की जड़ और गहरी हो सकती है।
कोर्ट ने यह चिंता जताई कि कई अल्पसंख्यक स्कूल RTE अधिनियम द्वारा निर्धारित सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं। इसके कारण वहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थी समानता और पहचान की भावना से वंचित हो रहे हैं।
कोर्ट ने कहा, “RTE अधिनियम से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट देना समान शिक्षा की कल्पना को खत्म करता है और अनुच्छेद 21A की समावेशिता और सार्वभौमिकता की भावना को कमजोर करता है। यह बच्चों को जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के आधार पर जोड़ने के बजाय विभाजन को बढ़ाता है और साझा शिक्षण स्थानों की बेहतर क्षमता को कम करता है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) RTE अधिनियम के तहत एक अनिवार्य शर्त है।गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इसे उत्तीर्ण करना जरूरी होगा।
प्रमति मामले के फैसले का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि इससे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है, न कि उन्हें सार्वभौमिक मानकों से अलग कर एक अलग प्रणाली में चलाना।
मान्यता मिली तो समानता भी दें शिक्षण संस्थान
कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के मामलों में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, लेकिन जब वे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करते हैं और राज्य से मान्यता, संबद्धता या सहायता प्राप्त करते हैं तो उन्हें समावेशी और शिक्षित समाज के निर्माण के लिए भी एक समान व्यवहार करना चाहिए और व्यापक संवैधानिक परियोजना में भाग लेना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रमति का निर्णय केवल RTE की धारा 12(1)(c) पर आधारित था। इसमें कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने की बात शामिल की गई है। जबकि शिक्षक योग्यता, संरचनात्मक मानक और बाल सुरक्षा उपायों जैसे मानकों पर इस फैसले में कोई चर्चा नहीं की गई।
कोर्ट के अनुसार, धारा 12(1)(c) का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 25% कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चे किसी विशेष या अन्य धर्म या भाषा वाले हों। यदि अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर या सामाजिक रूप से वंचित बच्चे इस कोटे के तहत प्रवेश लेते हैं तो क्या वास्तव में इसकी संख्या पर प्रश्न उठता है?
कोर्ट ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों के न्यूनतम नामांकन पर स्पष्ट दिशानिर्देश न होने के कारण ही संस्थान बेरोकटोक अल्पसंख्यक दर्जा लेने में आगे बढ़ गए हैं।
4 सवालों पर होगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम सवालों को बड़ी पीठ के समक्ष रखा है, जिनमें यह शामिल है कि क्या RTE की धारा 12(1)(c) को इस तरह पढ़ा जा सकता है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर भी वंचित वर्गों को लाभ पहुँचाए। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या 2014 का फैसला संविधान की मूल भावना के अनुरूप है?
इसके अलावा इसमें प्रमति फैसले से जुड़े दो सवाल भी हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रमति मामले में लिया गया फैसला RTE अधिनियम को अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ घोषित किया जाना उचित था? साथ ही क्या संस्थानों के RTE की छूट के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए?
यह मामला अब संविधान पीठ के समक्ष जाएगा, जो यह तय करेगी कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE से पूरी तरह छूट देना न्यायसंगत है या नहीं। इस फैसले का असर देश भर के लाखों बच्चों की शिक्षा और सामाजिक समावेशिता पर पड़ सकता है।